प्रस्तुति---एस.अनामिका श्रुति जारूहार
खोजी पत्रकारिता के लिए अक्सर तकनीकी हुनर, अच्छे संपर्क, संसाधन और साहस की ज़रूरत होती है. ऐसी नई रिपोर्टों पर काम करने वाले रिपोर्टरों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सूत्र सही हैं और रिपोर्ट में सच बात कही जा रही है. उन्हें विषय के हर पहलू को समझना होगा और अपनी जाँच के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए आधार तैयार करना होगा. बीबीसी के अनुभवी खोजी रिपोर्टर यहाँ बता रहे हैं कि इन विषयों को कैसे खोजा जाता है और कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है.
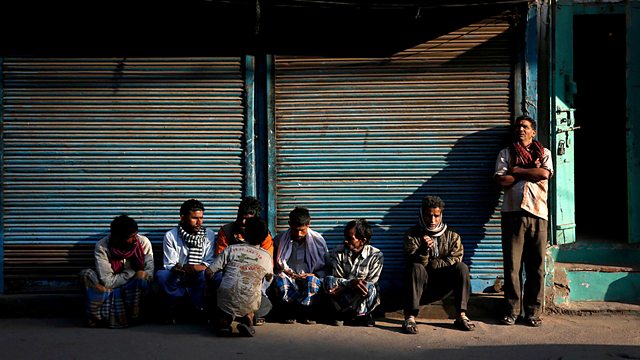
पत्रकारिता के पेश में खोजी पत्रकारिता को बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित काम माना जाता है. मगर ये काफ़ी मुश्किल काम है. इसमें तथ्य आधे-अधूरे होते हैं, गुमनाम स्रोतों से जानकारियाँ आती हैं, लीक हुए दस्तावेज़ होते हैं जिनकी प्रामाणिकता जाँचना कठिन होता है, यानी सच सामने नहीं होता, उसे सामने लाना पड़ता है. बीबीसी के नामी पत्रकार मैट प्रॉजर बताते हैं कि खोजी पत्रकारिता के लिए किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है.रिसर्च
किसी भी खोजी रिपोर्ट के लिए सबसे पहले गहराई से विषय के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है.
जितने अधिक लोगों से, जितनी अधिक जानकारी जुटाई जा सके रिपोर्ट उतनी ही सटीक होगी.
यह काम काफ़ी कठिन है, इसमें समय भी लगता है, पैसे भी ख़र्च होते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीक़ा नहीं है, अलग अलग विचारों को सामने रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है.गोपनीयता
अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को सच पता होता है वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते.
तो फिर आप ऐसे लोगों का इस्तेमाल कैसे करेंगे जो घबराहट की वजह से बिना सामने आए अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं?
इसके बारे में मैट प्रॉजर की सलाह है--
हर बातचीत से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह बातचीत ऑन रिकॉर्ड है या ऑफ़ द रिकॉर्ड, जानकारी देने वाले व्यक्ति को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि जिस शर्त पर और जिस काम के लिए जानकारी ली जा रही है उसका वैसे ही इस्तेमाल होगा.
ऑफ़ द रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आप उनका ज़िक्र अपनी रिपोर्ट में इस तरह नहीं करेंगे कि उनकी पहचान हो सके. आपने उनसे बात की है यह बात आप गोपनीय रखेंगे.
यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ हुई बातचीत का पूरा विवरण नोट करें, अपने सारे सूत्रों के नाम, घर के पते, मोबाइल नंबर वग़ैरह सुरक्षित रखें.निष्पक्षता
अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग आपसे बात करने को राज़ी होते हैं, इसके पीछे उनका उद्देश्य सही नहीं होता, कई बार बदले की भावना, राजनीतिक द्वेष या निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं. इसके अलावा ये भी होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का आरोप है वह भी बात करने से इनकार कर दे. ऐसे में आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से एकतरफ़ा और पक्षपातपूर्ण हो जाएगी.
किसी मंत्री की निंदा करने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं होती, अगर मंत्री बात करने को राज़ी न हो, और आपको स्टोरी करनी हो तो आपको ऐसे लोगों को खोजना होगा जिनकी सहानुभूति उस मंत्री के प्रति हो ताकि दूसरा पक्ष भी शामिल हो सके और पूरी रिपोर्ट संतुलित और निष्पक्ष हो.
खोजी रिपोर्टें आम तौर पर गंभीर होती हैं और उनके परिणाम काफ़ी बड़े हो सकते हैं, इसीलिए उनका असर भी होता है. अक्सर खोजी रिपोर्टिंग की शुरूआत से का़नूनी विशेषज्ञ की सलाह ली जानी चाहिए.
खोजी रिपोर्ट के ज़रिए आपका मक़सद सच जानना है, यह किसी को नुक़सान पहुँचाने का या शिकार करने जैसा मिशन नहीं होना चाहिए.प्रसारण
कुछ एडिटर खोजी रिपोर्टों को प्रकाशित या प्रसारित करने से घबराते हैं, पहले तो इसमें समय लगता है, पैसे ख़र्च होते हैं फिर भी गारंटी नहीं होती कि स्टोरी कारगर होगी. ऊपर से ऐसे मामलों में मुकदमे का भी जोखिम रहता है, इसलिए कई संपादक इस तरह की रिपोर्टों से कतराते हैं.
ज़रूरी है कि आपके पास पूरे सबूत, पूरी जानकारी हो, एक खोजी रिपोर्ट एक मुकदमा लड़ने की तैयारी से कम नहीं होती जिसमें पूरी विस्तृत फ़ाइल तैयार की जाती है. सिर्फ़ ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा कि ‘दाल में काला है’,‘मुझे शक है’, ‘मैं दावे से कह सकता हूँ’.
काम कठिन है, धीरज वाला है और तत्काल कोई परिणाम नहीं मिलता लेकिन एक बार जब आपकी रिपोर्ट प्रसारित होती है उसका असर ज़रूर होता है जो एक पत्रकार के लिए बहुत सुखद है.