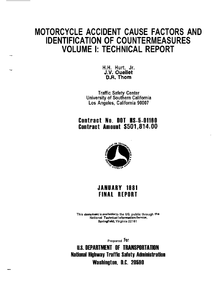मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया से
भारत,
संसदीय प्रणालीकी सरकार वाला एक प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य
भारत के संविधानके अनुसार शासित है। भारत का संविधान
संविधान सभाद्वारा 26 नवम्बर, 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी का दिन भारत में
गणतन्त्र दिवसके रूप में मनाया जाता है।
संक्षिप्त परिचय
भारत का संविधान दुनिया का सबसे बडा लिखित संविधान है। इसमें 444 अनुच्छेद,तथा १२ अनुसूचियां हैं। परन्तु इसके निर्माण के समय इसमें केवल ८ अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख
राष्ट्रपतिहै। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय
संसदकी परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद्
राज्यसभातथा लोगों का सदन
लोकसभाके नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रमुख
प्रधान मंत्रीहोगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में मनमोहन सिंह हैं।
मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक
विधान सभाहै। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में एक ऊपरी सदन है जिसे
विधान परिषद्कहा जाता है।
राज्यपालराज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें विहित होगी। मंत्रिपरिषद्, जिसका प्रमुख
मुख्य मंत्रीहै, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू- भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है।
अनुसूचियाँ
1. पहली अनुसूची - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन ।
2. दूसरी अनुसूची - [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] - मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते भाग-क-राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते, भाग-ख- लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,भाग-ग- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते, भाग-घ- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षकके वेतन-भत्ते।
3. तीसरी अनुसूची - [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।
4. चौथी अनुसूची - [अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।
5. पाँचवी अनुसूची - [अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।
6. छठी अनुसूची - [अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय मे उपबंध।
7. सातवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 246] - विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।
8. आठवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाएँ - 22 भाषाओं का उल्लेख।
9. नवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 31 ख ] - कुछ भुमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।
10.दसवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर अ
११ ग्यारवी अनुसूची - पन्चायती राज से सम्बन्धित
१२ बारह्ववी अनुसूची - यह अनुसूची संविधान मे ७४ वे संवेधानिक संशोंधन द्वारा जोडि गई।
इतिहास
द्वितीय विश्वयुद्धकी समाप्ति के बाद जुलाई १९४५ में
ब्रिटेनने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक
कैबिनेट मिशनभारत भेजा जिसमें ३ मंत्री थे। १५ अगस्त, १९४७ को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद
संविधान सभाकी घोषणा हुई और इसने अपना कार्य ९ दिसम्बर १९४६ से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे।
जवाहरलाल नेहरू, डॉ
राजेन्द्र प्रसाद, सरदार
वल्लभ भाई पटेल,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना
अबुल कलाम आजादआदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने २ वर्ष, ११ माह, १८ दिन मे कुल १६६ दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में डॉ
भीमराव अंबेदकरने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्होंने संविधान का निर्माता कहा जाता है।
भारतीय संविधान की प्रकृति
संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने इस को संघात्मक संविधान माना है, परन्तु विद्वानों में मतभेद है । अमेरीकी विद्वान इस को छदम-संघात्मक-संविधान कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते है कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता । संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय (पि कन्नादासन वाद) ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है ।
आधारभूत विशेषताएं
१
शक्ति विभाजन -यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है , राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों मे विभाजित होती है शक्ति विभाजन के चलते द्वेध सत्ता [केन्द्र-राज्य सत्ता ] होती है
दोनों सत्ताएँ एक-दूसरे के अधीन नही होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती है दोनों की सत्ता अपने अपने क्षेत्रो मे पूर्ण होती है
२
संविधान की सर्वोचता - संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते है [केन्द्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद
1 अनुच्छेद 54,55,73,162,241
2 भाग -5 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य तथा केन्द्र के मध्य वैधानिक संबंध
3 अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची
4 राज्यो का संसद मे प्रतिनिधित्व
5 संविधान मे संशोधन की शक्ति अनु 368इन सभी अनुच्छेदो मे संसद अकेले संशोधन नही ला सकती है उसे राज्यो की सहमति भी चाहिए
अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से सम्बन्धित नही है
3 लिखित सविन्धान अनिवार्य रूप से लिखित रूप मे होगा क्योंकि उसमे शक्ति विभाजन का स्पषट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ मे लिखित संविधान अवश्य होगा
4 सविन्धान की कठोरता इसका अर्थ है सविन्धान संशोधन मे राज्य केन्द्र दोनो भाग लेंगे
5
न्यायालयो की अधिकारिता- इसका अर्थ है कि केन्द्र-राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे
विधि द्वारा स्थापित 1.1 न्यायालय ही संघ-राज्य शक्तियो के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे
1.2 न्यायालय सविन्धान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे भारत मे यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है ये पांच शर्ते किसी सविन्धान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य है
भारत मे ये पांचों लक्षण सविन्धान मे मौजूद है अत्ः यह संघात्मक है परंतु
भारतीय संविधान मे कुछ विभेदकारी विशेषताए भी है
1 यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है
2 राज्य अपना पृथक संविधान नही रख सकते है, केवल एक ही संविधान केन्द्र तथा राज्य दोनो पर लागू होता है
3 भारत मे द्वैध नागरिकता नही है। केवल भारतीय नागरिकता है
4 भारतीय संविधान मे आपातकाल लागू करने के उपबन्ध है [352 अनुच्छेद] के लागू होने पर राज्य-केन्द्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जायेगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जायेगा। इस स्थिति मे केन्द्र-राज्यों पर पूर्ण सम्प्रभु हो जाता है
5 राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केन्द्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है [बिना राज्यों की सहमति से] [अनुच्छेद 3] अत: राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नही हैं। केन्द्र संघ को पुर्ननिर्मित कर सकती है
6 संविधान की 7
वींअनुसूची मे तीन सूचियाँ हैं
संघीय,
राज्य, तथा
समवर्ती। इनके विषयों का वितरण केन्द्र के पक्ष मे है
6.1 संघीय सूची मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं
6.2 इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है
6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण हैं, 5 विशेष परिस्थितियों मे राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है किंतु किसी एक भी परिस्थिति मे राज्य केन्द्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते
क1 अनु 249—राज्य सभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित हेतु यह आवश्यक है [2\3 बहुमत से] किंतु यह बन्धन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू होता है
क2 अनु 250— राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वत: मिल जाता है
क3 अनु 252—दो या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है [केवल संबंधित राज्यों पर]
क4 अनु253--- अंतराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है
क5 अनु 356—जब किसी राज्य मे
राष्ट्रपति शासनलागू होता है, उस स्थिति मे संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है
7 अनुच्छेद 155 – राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णत: केन्द्र की इच्छा से होती है इस प्रकार केन्द्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है
8 अनु 360 – वित्तीय आपातकाल की दशा मे राज्यों के वित्त पर भी केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा मे केन्द्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है
9 प्रशासनिक निर्देश [अनु 256-257] -केन्द्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाये, के बारे मे निर्देश दे सकता है, ये निर्देश किसी भी समय दिये जा सकते है, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य मे संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है
10 अनु 312 मे अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों मे पूर्णत: केन्द्र के अधीन है जबकि ये सेवा राज्यों मे देते है राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है
11 एकीकृत न्यायपालिका
12 राज्यों की कार्यपालिक शक्तियां संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नही हो सकती है।
संविधान की प्रस्तावना
संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व मे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह ‘हम भारत के लोग’ इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद मे कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नही करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नही कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है।
संविधान की प्रस्तावना:- " हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा
- उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए
- दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद
- द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"
संविधान के तीन भाग
संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं। भाग एक में संघ तथा उसका राज्यक्षेत्रों के विषय में टिप्पणीं की गई है तथा यह बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। विदेश में रहने वाले कौन लोग भारतीय नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है। • संविधान की प्रस्तावना बाहर सेट मुख्य उद्देश्य है जो संविधान सभा को प्राप्त करने का इरादा है. • 'उद्देश्य' संकल्प पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित है और संविधान सभा द्वारा पारित, अंततः भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया. • जैसा कि
उच्चतम न्यायालयने मनाया है, प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है. • यह भी भारत के लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है. • संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 प्रस्तावना में संशोधन और शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रस्तावना के लिए वफ़ादारी जोड़ी. • प्रस्तावना प्रकृति में गैर न्यायोचित है, राज्य के नीति theDirective सिद्धांतों की तरह और कानून की एक अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है. यह न तो राज्य के तीन अंगों को मूल शक्ति (निश्चित और वास्तविक शक्ति) प्रदान कर सकते हैं, और न ही संविधान के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों की सीमा. • संविधान की प्रस्तावना विशिष्ट प्रावधान नहीं ओवरराइड कर सकते हैं. दोनों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में, बाद अभिभावी होगी. तो •, यह एक बहुत ही सीमित भूमिका निभानी है. •
उच्चतम न्यायालयने मनाया प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों के आसपास अस्पष्टता को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
प्रस्तावना के प्रयोजन
• प्रस्तावना वाणी है कि यह भारत के लोगों को जो अधिनियमित था अपनाया और खुद को संविधान दिया है. • इस प्रकार, संप्रभुता लोगों के साथ अंत में निहित है. • यह भी लोगों की जरूरत है कि प्राप्त किया जा करने के आदर्शों और आकांक्षाओं को वाणी है. • आदर्शों आकांक्षाओं से अलग कर रहे हैं. जबकि पूर्व हे परमेश्वर के रूप में भारत के संविधान की घोषणा के साथ हासिल किया गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, जो अभी तक प्राप्त किया जा शामिल है. आदर्शों आकांक्षाओं को प्राप्त करने का मतलब हैं.
प्रस्तावना
हम, भारत के लोगों, सत्यनिष्ठा से एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत का गठन करने के लिए और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित हल होने: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक; सोचा, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति के और अवसर की समानता, और उन सब के बीच बढ़ावा देने व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा आश्वस्त बिरादरी; हमारी संविधान सभा नवम्बर, 1949 के इस बीस छठे दिन में, एतद्द्वारा, अपनाने करते अधिनियमित और अपने आप को इस संविधान दे.
प्रभु 'संप्रभु' शब्द पर जोर दिया कि भारत के बाहर कोई अधिकार नहीं है जिस पर देश के किसी भी निर्भर रास्ते में है.
समाजवादी 'समाजवादी' शब्द करके, संविधान लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाज के समाजवादी पैटर्न की उपलब्धि का मतलब है.
लौकिक • है कि भारत एक 'सेकुलर राज्य' है का मतलब है कि भारत के गैर - धार्मिक या अधार्मिक, या विरोधी धार्मिक नहीं करता, लेकिन बस है कि राज्य में ही धार्मिक और नहीं है "सर्व धर्म Samabhava" प्राचीन भारतीय सिद्धांत निम्नानुसार है. • यह भी मतलब है कि राज्य के नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा. • राज्य का संबंध धर्म विश्वास करने के लिए सही है या नहीं एक धर्म में विश्वास सहित एक व्यक्ति का निजी मामला हो सकता है. हालांकि, भारत अर्थ है पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, अपनी विशिष्ट सामाजिक - सांस्कृतिक वातावरण के कारण.
यह संविधान का एक हिस्सा है? • Kesavananda केरल मामले (1971) की भारती बनाम राज्य में
उच्चतम न्यायालयके 1960 के पहले निर्णय खारिज (Berubari मामले) और यह स्पष्ट है कि यह संविधान का एक हिस्सा है और संसद के संशोधन के रूप में सत्ता के अधीन है संविधान के किसी अन्य प्रावधान, संविधान के मूल ढांचे प्रदान के रूप में प्रस्तावना में पाया नष्ट नहीं है. हालांकि, यह संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है. • नवीनतम S.R. बोम्मई मामले में, 1993 में तीन सांसद, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी के बारे में, जस्टिस रामास्वामी ने कहा, "संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है सरकार, संघीय ढांचे की एकता और अखंडता के लोकतांत्रिक रूप. राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा संविधान के बुनियादी सुविधाओं कर रहे हैं ". • प्रश्न प्रस्तावना जब यह एक बुनियादी सुविधा है संशोधन किया गया था क्यों के रूप में उठता है. 42 संशोधन करके, प्रस्तावना 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था के रूप में यह मान लिया था कि इन संशोधनों को स्पष्ट कर रहे हैं और प्रकृति में योग्यता. वे पहले से ही प्रस्तावना में निहित हैं
लोकतंत्रीय • शब्द का अर्थ है 'डेमोक्रेटिक कि लोगों द्वारा चुने गए शासकों केवल सरकार चलाने का अधिकार है. • भारत 'प्रतिनिधि लोकतंत्र' की एक प्रणाली है, जहां सांसदों और विधायकों को सीधे लोगों द्वारा चुने गए हैं निम्नानुसार है. पंचायतों और नगर पालिकाओं (73 और 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992) के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र ले • प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, प्रस्तावना न केवल राजनीतिक, लेकिन यह भी लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्रों की परिकल्पना की गई है.
गणतंत्र 'गणतंत्र' शब्द का मतलब है कि वहाँ भारत में कोई वंशानुगत शासक और राज्य के सभी प्राधिकारी हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने गए मौजूद है.
प्रस्तावना राज्यों है कि प्रत्येक नागरिक उद्देश्यों के लिए सुरक्षित कर रहे हैं 1. न्यायमूर्ति: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक • न्याय के बारे में, एक बात स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक न्याय के लिए राज्य और अधिक से अधिक कल्याण प्रकृति में उन्मुख बनाने के द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने का मतलब हो जाने की उम्मीद है. • भारत में राजनीतिक न्याय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा योग्यता के किसी भी प्रकार के बिना गारंटी है. • जबकि सामाजिक न्याय सम्मान की abolishingjmy Jitle (18 Art.) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और अस्पृश्यता (17 Art.), निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से मुख्य रूप से आर्थिक न्याय की गारंटी है.
2. लिबर्टी: सोचा, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की • लिबर्टी एक मुक्त समाज का एक अनिवार्य विशेषता है कि एक व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक संकायों के पूर्ण विकास में मदद करता है. • भारतीय संविधान छह आर्ट के तहत व्यक्तियों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है. 19 और धर्म की कला के तहत स्वतंत्रता का अधिकार. 25-28.
3. की स्थिति, अवसर: समानता • स्वतंत्रता का फल पूरी तरह से जब तक वहाँ स्थिति और अवसर की समानता है महसूस नहीं किया जा सकता है. • हमारा संविधान यह गैरकानूनी बना देता है, धर्म, जाति, लिंग, या सभी के लिए खुला सार्वजनिक स्थानों अस्पृश्यता (17 Art.) को खत्म करने, फेंकने द्वारा और जन्म स्थान (15 Art.) के आधार पर ही राज्य द्वारा किसी भेदभाव सम्मान के खत्म शीर्षक (ArtJ8). • हालांकि, राष्ट्रीय मुख्यधारा में समाज के अब तक उपेक्षित वर्गों को लाने के लिए, संसद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों (सुरक्षा भेदभाव) के लिए कुछ कानून पारित कर दिया गया है.
4. बिरादरी भाईचारे के रूप में संविधान में निहित भाईचारे की भावना लोगों के सभी वर्गों के बीच प्रचलित मतलब है. यह राज्य धर्मनिरपेक्ष बनाने, समान रूप से सभी वर्गों के लोगों को मौलिक और अन्य अधिकारों की गारंटी, और उनके हितों की रक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा मांग की है. हालांकि, बिरादरी एक उभरती प्रक्रिया है और 42 संशोधन द्वारा 'अखंडता' शब्द जोड़ा गया था, इस प्रकार यह एक व्यापक अर्थ दे.
के.एम. मुंशी 'राजनीतिक कुंडली' के रूप में करार दिया. बयाना बार्कर यह संविधान की कुंजी कहता है. ठाकुरदास भार्गव 'संविधान की आत्मा' के रूप में मान्यता दी. शब्द 'समाज के सोशलिस्टिक पैटर्न' अवादी सत्र में 1955 में कांग्रेस द्वारा भारतीय राज्य का एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था.
संविधान भाग ५ नीति निर्देशक तत्व
भाग 3 तथा 4 मिल कर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैक्यों कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा निति निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं सर्वप्रथम ये
आयरलैंडके संविधान मे लागू किये गये थे। ये वे तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए है। इन तत्वॉ का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व मे भेद बताया गया है और नीति निदेशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है।
भाग 4 क मूल कर्तव्य
मूल कर्तव्य मूल सविधान में नहीं थे, इन्हे ४२ वें संविधान संशोधन द्ववारा जोड़ा गया है। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गये तथा संविधान के भाग ४ (क) के अनुच्छेद ५१ - अ मे रखे गये हैं । ये कुल ११ है ।
51 क. मूल कर्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-
(क) संविधान का पालन करे और उस के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ; (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उन का पालन करे; (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे; (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान करने किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे; (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है; (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उस का परिरक्षण करे; (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिस के अंतर्गत वन, झील नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उस का संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे; (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे; (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिस से राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले; (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।
भाग 5 संघ
पाठ 1 संघीय कार्यपालिका
संघीय कार्यपालिका मे राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति,मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आते है। रामजवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य वाद मे सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका शक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है-
- 1 विधायिका न्यायपालिका के कार्यॉ को पृथक करने के पश्चात सरकार का बचा कार्य ही कार्यपालिका है।
- 2 कार्यपालिका मॅ देश का प्रशासन, विधियॉ का पालन सरकारी नीति का निर्धारण ,विधेयकॉ की तैयारी करना ,कानून व्यव्स्था बनाये रखना सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढावा देना विदेश नीति निर्धारित करना आदि आता है।
राष्ट्रपति
संघ का कार्यपालक अध्यक्ष है संघ के सभी कार्यपालक कार्य उस के नाम से किये जाते है अनु 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उसमॅ निहित है इन शक्तियॉ/कार्यों का प्रयोग क्रियांवय्न राष्ट्रपति सविन्धान के अनुरूप ही सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियॉ के माध्यम से करेगा। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है,सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है वह देश का प्रथम नागरिक है तथा राज्य द्वारा जारी वरीयता क्रम मे उसका सदैव प्रथम स्थान होता है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है तथा उसकी आयु कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव, उस पर महाभियोग की अवस्थाएँ, उसकी शक्तियाँ, संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति तथा राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।
उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना--उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा: परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।
65. राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन--(1) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।
(2) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।
उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।
66. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन--(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।
(2) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
(3) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह-- (क) भारत का नागरिक है, (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और (ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।
(4) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल 2 * * * है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।
67. उपराष्ट्रपति की पदावधि--(1) उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंतु-- (क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; (ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो; (ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। 68. उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि--(1) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। (2) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।
69. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान--प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्: -- ईश्वर की शपथ लेता हूँ
मैं, अमुक ---------------------------------कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।मंत्रिपरिषद
संसदीय लोकतंत्र के मह्त्वपूर्ण सिद्धांत 1. राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख न होकर मात्र संवैधानिक प्रमुख ही होता है
2. वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, मंत्रिपरिषद जो कि सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के सामने उत्तरदायी होगा के पास होगी
3 मंत्रिपरिषद के सद्स्य संसद के सद्स्यों से लिए जायेंगे
परिषद का गठन
1. प्रधानमंत्री के पद पे आते ही यह परिषद गठित हो जाती है यह आवश्यक नही है कि उसके साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ ले केवल प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद होगा
2 मंत्रिपरिषद की सद्स्य संख्या पर मौलिक संविधान मे कोई रोक नही थी किंतु 91 वे संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या
लोकसभा के सद्स्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गयी वही राज्यों मेभी मंत्रीपरिषद की
संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नही होगी पंरंतु न्यूनतम 12 मंत्री होंगे
मंत्रियों की श्रेणियाँ
संविधान मंत्रियों की श्रेणी निर्धारित नही करता यह निर्धारण अंग्रेजी प्रथा के आधार पर किया गया है
कुल ती
ड़्न प्रकार के मंत्री माने गये है
- 1. कैबिनेट मंत्री—सर्वाधिक वरिष्ठ मंत्री है उनसे ही कैबिनेट का गठन होता है मंत्रालय मिलने पर वे उसके अध्यक्ष होते है उनकी सहायता हेतु राज्य मंत्री तथा उपमंत्री होते है उन्हें कैबिनेट बैठक मे बैठने का अधिकार होता है अनु 352 उन्हें मान्यता देता है
कृप्या सभी कैबिनेट मंत्रालयों ,राज्य मंत्रालय की सूची पृथक से जोड दे- 2. राज्य मंत्रीद्वितीय स्तर के मंत्री होते है सामान्यत उनहे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमंत्री चाहे तो यह कर सकता है उन्हें कैबिनेट बैठक मे आने का अधिकार नही होता।
- 3. उपमंत्रीकनिष्ठतम मंत्री है उनका पद सृजन कैबिनेट या राज्य मंत्री को सहायता देने हेतु किया जाता है वे मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी नही लेते है।
- 4. संसदीय सचिवसत्तारूढ दल के संसद सद्स्य होते है इस पद पे नियुक्त होने के पश्चात वे मंत्री गण की संसद तथा इसकी समितियॉ मे कार्य करने मे सहायता देते है वे प्रधान मंत्री की इच्छा से पद ग्रहण करते है वे पद गोपनीयता की शपथ भी प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रहण करते है वास्तव मे वे मंत्री परिषद के सद्स्य नही होते है केवल मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
मंत्रिमंडल
मंत्रि परिषद एक संयुक्त निकाय है जिसमॆं 1,2,या 3 प्रकार के मंत्री होते है यह बहुत कम मिलता है चर्चा करता है या निर्णय लेता है वहीं मंत्रिमंडल मे मात्र कैबिनेट प्रकार के मंत्री होते है यह समय समय पर मिलती है तथा समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लेती है इस के द्वारा स्वीकृत निर्णय अपने आप परिषद द्वारा स्वीकृत निर्णय मान लिये जाते है यही देश का सर्वाधिक मह्त्वपूर्ण निर्णय लेने वाला निकाय है
- सम्मिलित उत्तरदायित्वअनु 75[3] के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद के सामने सम्मिलित रूप से उत्तरदायी है इसका लक्ष्य मंत्रिपरिषद मे संगति लाना है ताकि उसमे आंतरिक रूप से विवाद पैदा ना हो।
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्वअनु 75[2] के अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के सामने उत्तरदायी होते है किंतु यदि प्रधानमंत्री की सलाह ना हो तो राष्ट्रपति मंत्री को पद्च्युत नही कर सकता है।
भारत का महान्यायवादी
भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य न रहते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है ।
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की दशा समानों मे प्रधान की तरह है वह कैबिनेट का मुख्य स्तंभ है मंत्री परिषद का मुख्य सद्स्य भी वही है अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
प्रधानमंत्री सरकार के प्रकारप्रधानमंत्री सरकार संसदीय सरकार का ही प्रकार है जिसमे प्रधानमंत्री मंत्रि परिषद का नेतृत्व करता है वह कैबिनेट की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है वह कैबिनेट से अधिक शक्तिशाली है उसके निर्णय ही कैबिनेट के निर्णय है देश की सामान्य नीतियाँ कैबिनेट द्वारा निर्धारित नहीं होती है यह कार्य प्रधानमंत्री अपने निकट सहयोगी चाहे वो मंत्रि परिषद के सद्स्य ना हो की सहायता से करता है जैसे कि इंदिरा गाँधी अपने किचन कैबिनेट की सहायता से करती थी
प्रधानमंत्री सरकार के लाभ
- 1 तीव्र तथा कठोर निर्णय ले सकती है
- 2 देश को राजनैतिक स्थाईत्व मिलता है
इससे कुछ हानि भी है
- 1 कैबिनेट ऐसे निर्णय लेती है जो सत्ता रूढ दल के हित मे हो न कि देश के हित मे
- 2 इस के द्वारा गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रों का जन्म होता है
कैबिनेट सरकारसंसदीय सरकार का ही प्रकार है इस मे नीति गत निर्णय सामूहिक रूप से कैबिनेट [मंत्रि मंडल ] लेता है इस मे प्रधानमंत्री कैबिनेट पे छा नही जाता है इस के निर्णय सामान्यत संतुलित होते है लेकिन कभी कभी वे इस तरह के होते है जो अस्पष्ट तथा साहसिक नही होते है। 1989 के बाद देश मे प्रधानमंत्री प्रकार का नही बल्कि कैबिनेट प्रकार का शासन रहा है।
प्रधानमन्त्री के कार्य१- मन्त्रीपरिषद के गठन का कार्य २- प्रमुख शासक ३- नीति निर्माता ४- ससद का नेता ५- विदेश निती का निर्धारक
कार्यकारी सरकार
बहुमत समाप्त हो जाने के बाद जब मंत्रि परिषद त्यागपत्र दे देती है तब कार्यकारी सरकार अस्तित्व मे आती है अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु/ त्यागपत्र की दशा मे यह स्थिति आती है। यह सरकार अंतरिम प्रकृति की होती है यह तब तक स्थापित रहती है जब तक नयी मंत्रिपरिषद शपथ ना ले ले यह इसलिए काम करती है ताकि अनुच्छेद 74 के अनुरूप एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता हेतु रहे। वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद में
उच्चतम न्यायालयने माना था कि मंत्रि परिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए यदि यह अनुपस्थित हुई तो राष्ट्रपति अपने काम स्वंय करने लगेगा जिस से सरकार का रूप बदल कर राष्ट्रपति हो जायेगा जो कि संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होगा। यह कार्यकारी सरकार कोई भी वित्तीय/नीतिगत निर्णय नही ले सकती है क्योंकि उस समय लोक सभा मौजूद नही रहती है वह केवल देश का दैनिक प्रशासन चलाती है। इस प्रकार की सरकार के सामने सबसे विकट स्थिति तब आ गयी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 1999 मे कारगिल युद्ध का संचालन करना पडा था। किंतु विकट दशा मे इस प्रकार की सरकार भी कोई भी नीति निर्णय ले सकती है।
सुस्थापित परंपराए
एक संसदीय सरकार में ये पंरपराए ऐसी प्रथाएँ मानी जाती है जो सरकार के सभी अंगों पर वैधानिक रूप
से लागू मानी जाती है उनका वर्णन करने के लिये कोई विधान नहीं होता है ना ही संविधान मे किसी देश के शासन के बारे मे पूर्ण वर्णन किया जा सकता है संविधान निर्माता भविष्य मे होने वाले विकास तथा देश के शासन पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकते अतः वे उनके संबंध मे संविधान में प्रावधान भी नहीं कर सकते है
इस तरह संविधान एक जीवित शरीर तो है परंतु पूर्ण वर्णन नही है इस वर्णन मे बिना संशोधन लाये परिवर्तन भी नहीं हो सकता है वही पंरपराए संविधान के प्रावधानॉ की तरह वैधानिक नहीं होती वे सरकार के संचालन में स्नेहक का कार्य करते है तथा सरकार का प्रभावी संचालन करने मे सहायक है
पंरपराए इस लिए पालित की जाती है क्योंकि उनके अभाव मे राजनैतिक कठिनाइया आ सकती है इसी कारण उन्हें संविधान का पूरक माना जाता हैब्रिटेन मे हम इनका सबसे विकसित तथा प्रभावशाली रूप देख सकते है
इनके दो प्रकार है प्रथम वे जो संसद तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संयोजन का कार्य करती है यथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर परिषद का त्यागपत्र दे देना
द्वितीय वे जो विधायिका की कार्यवाहिय़ों से संबंधित है जैसे किसी बिल का तीन बार वाचन संसद के तीन सत्र राष्ट्रपति द्वारा धन बिल को स्वीकृति देना उपस्पीकर का चुनाव विपक्ष से करना जब स्पीकर सत्ता पक्ष से चुना गया हो आदि
सरकार के संसदीय तथा राष्ट्रपति प्रकारसंसदीय शासन के समर्थन मे तर्क1. राष्ट्रपतीय शासन मे राष्ट्रपति वास्तविक कार्य पालिका होता है जो जनता द्वारा निश्चित समय के लिये चुना जाता है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नेही होता है उसके मंत्री भी विधायिका के सदस्य नही होते है तथा उसी के प्रति उत्ततदायी होंगे न कि विधायिका के प्रति
वही संसदीय शासन मे शक्ति मंत्रि परिषद के पास होती है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है
2. भारत की विविधता को देखते हुए संसदीय शासन ज्यादा उपयोगी है इस मे देश के सभी वर्गों के लोग मंत्रि परिषद मे लिये जा सकते है
3. इस् शासन मे संघर्ष होने [विधायिका तथा मंत्रि परिषद के मध्य] की संभावना कम रहती है क्यॉकि मंत्री विधायिका के सदस्य भी होते है
4 भारत जैसे विविधता पूर्ण देश मे सर्वमान्य रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करना लगभग असंभव है
5 मिंटे मार्ले सुधार 1909 के समय से ही संसदीय शासन से भारत के लोग परिचय रखते है ,kfduytjkjoojidsfuhgyuhgihtriijik
भाग पाँच, अध्याय 2, संसद
राज्य सभा
राज्यों को संघीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देने वाली सभा है जिसका कार्य संघीय स्तर पर राज्य हितॉ का संरक्षण करना है। इसे संसद का दूसरा सदन कह्ते है इसके सदस्य दो प्रकार से निर्वाचित होते है राज्यॉ से 238 को निर्वाचित करते है तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 को मनोनीत करते है। वर्तमान मे यह संख्या क्रमश 233 ,12 है ये सद्स्य 6 वर्ष हेतु चुने जाते है इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है मत एकल संक्रमणीय प्रणाली से डाले जाते है। मत खुले डाले जाते है.सद्स्य जो निर्वाच्त होना चाहते है देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र से एक निर्वाचक के रूप मे पंजीकृत होने चाहिए।
राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ
राज्यसभा के पास तीन विशेष शक्तिया होती है
- अनु. 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक
- अनु. 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 2/3 बहुमत से करना
- अनु. 67 ब उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव राज्यसभा मे ही लाया जा सकेगा
राज्य सभा का संघीय स्वरूप
- राज्य सभा का गठन ही राज्य परिषद के रूप मे संविधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व देने के लिये हुआ था
- राज्य सभा के सद्स्य मंत्रि परिषद के सदस्य बन सकते है जिससे संघीय स्तर पर निर्णय लेने मे राज्य का प्रतिनिधित्व होगा
- राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मे समान रूप से भाग लेती है
- अनु 249,312 भी राज्य सभा के संघीय स्वरूप तथा राज्यॉ के संरक्षक रूप मे उभारते है
- सभी संविधान संशोधन बिल भी इस के द्वारा पृथक सभा कर तथा 2/3 बहुमत से पास होंगे
- संसद की स्वीकृति चाहने वाले सभी प्रस्ताव जो कि आपातकाल से जुडे हो भी राज्यसभा द्वारा पारित होंगे
राज्य सभा के गैर संघीय तत्व
- संघीय क्षेत्रॉ को भी राज्य सभा मे प्रतिनिधित्व मिलता है जिससे इसका स्वरूप गैर संघीय हो जाता है
- राज्यॉ का प्रतिनिधित्व राज्यॉ की समानता के आधार पे नही है जैसा कि अमेरिका मे है वहाँ प्रत्येक राज्य को
सीनेट मे दो स्थान मिलते है किंतु भारत मे स्थानॉ का आवंटन आबादी के आधार पे किया गया है - राज्य सभा मे मनोनीत सद्स्यों का प्रावधान है
राज्य सभा का मह्त्व
- किसी भी संघीय शासन मे संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितॉ की संघीय
स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है ,इसी कारण राज्य सभा को सदनॉ
की समानता के रूप मे देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप मे हुआ है - यह जनतंत्र की मांग है कि जहाँ लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है विशेष शक्तियॉ का उपभोग करती है
,लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के लिये बाध्य करते है किंतु ये दो कारण किसी भी प्रकार
से राज्यसभा का मह्त्व कम नही करते है - राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप मे हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावॉ की पुनरीक्षा करे
यह मंत्रिपरिषद मे विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस मे मनोनीत होते ही है - आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते है राज्य सभा द्वारा भी पास होने चाहिये
- राज्य सभा का महत्व यह है कि जहाँ लोकसभा सदैव सरकार से सहमत होती है जबकि राज्यसभा सरकार की नीतिय़ों का निष्पक्ष मूल्याँकन कर सकती है
- मात्र नैतिक प्रभाव सरकार पे डालती है किंतु यह लोकस्भा के प्रभाव की तुलना मे ज्यादा होता है
राज्य सभा के पदाधिकारी उनका निर्वाचन ,शक्ति ,कार्य, उत्तरदायित्व तथा पदच्युति
लोकसभा
यह संसद का लोकप्रिय सदन है जिसमे निर्वाचित मनोनीत सद्स्य होते है संविधान के अनुसार लोकसभा का विस्तार राज्यॉ से चुने गये 530, संघ क्षेत्र से चुने गये 20 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यॉ तक होगा वर्तमान मे राज्यॉ से 530 ,संघ क्षेत्रॉ
से 13 तथा 2 आंग्ल भारतीय सद्स्यॉ से सदन का गठन किया गया है
कुछ स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है
प्रत्येक राज्य को उसकी आबादी के आधार पर सद्स्य मिलते है अगली बार लोकसभा के सदस्यॉ की संख्या वर्ष 2026 मे निर्धारित किया जायेगा वर्तमान मे यह 1971 की जनसंख्या पे आधारित है इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे यह कार्य बकायदा 84 वे संविधान संशोधन से किया गया था ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नही करे
लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है पर्ंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है
लोकसभा की विशेष शक्तियाँ
- मंत्री परिषद केवल लोकस्भा के प्रति उत्तरदायी है अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरूद्ध केवल यही लाया जा सकता है
- धन बिल पारित करने मे यह निर्णायक सदन है
- राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकस्भा मे लाया और पास किया जायेगा
लोकसभा के पदाधिकारी
स्पीकर
लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसका चुनाव लोकसभा सदस्य अपने मध्य मे से करते है इसके दो कार्य है
1. लोकसभा की अध्यक्षता करना उस मे अनुसाशन गरिमा तथा प्रतिष्टा बनाये रखना इस कार्य हेतु वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नही होता है
2. वह लोकसभा से संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है किंतु इस भूमिका के रूप मे वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा
उसकी विशेष शक्तियाँ1. दोनो सदनॉ का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा उसके अनुउपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमाकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है
2. धन बिल का निर्धारण स्पीकर करता है यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही करता तो वह धन बिल ही नही माना जायेगा उसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी होगा
3. सभी संसदीय समितियाँ उसकी अधीनता मे काम करती है उसके किसी समिति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा
4. लोकसभा के विघटन होने पर भी उसका प्रतिनिधित्व करने के लिये स्पीकर पद पर कार्य करता रहता है नवीन लोकसभा चुने जाने पर वह अपना पद छोड देता है
स्पीकर प्रोटेम [कार्यवाहक]
जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है जिसको संसद मे सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है
उसके दो कार्य होते है1. संसद सदस्यॉ को शपथ दिलवाना
2. नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है
उपस्पीकर
विधायिका[संसद - राज्य विधायिका] मे बहुमत के प्रकार
1.
सामान्य बहुमत– उपस्थित सदस्यॉ तथा मतदान करने वालॉ के 50% से अधिक सदस्य ही सामान्य बहुमत है इस बहुमत का सदन की कुल सदस्य संख्या से कोई संबंध नही होता है
भारतीय संविधान के अनुसार
अविश्वास प्रस्ताव,
विश्वास प्रस्ताव,
कामरोको प्रस्ताव, सभापति ,उपसभापति तथा अध्यक्षॉ के चुनाव हेतु सदन के यदि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य विधायिकाओं को भेजना हो ,
सामान्य बिल ,
धन बिल,
राष्ट्रपति शासन ,
वित्तीय आपातकाललगाने हेतु सामान्य बहुमत को मान्यता प्राप्त है यदि बहुमत के प्रकार का निर्देश न होने पर उसे सदैव सामान्य बहुमत समझा जाता है
2.
पूर्ण बहुमत– सदन के 50% से अधिक सदस्यॉ का बहुमत [खाली सीटे भी गिनी जाती है] लोकसभा मे 273, राज्यसभा मे 123 सदस्यॉ का समर्थन . इसका राजनैतिक मह्त्व है न कि वैधानिक महत्व
3.
प्रभावी बहुमत- मतदान के समय उपस्थित सदन के 50% से अधिक सदस्यॉ [खाली सीटॉ को छोडकर] यह तब प्रयोग आती है जब लोक सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना हो या जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु मतदान करे
4.
विशेष बहुमत– प्रथम तीनो प्रकार के बहुमतॉ से भिन्न होता है इसके तीन प्रकार है
[क]
अनु 249 के अनुसार- उपस्थित तथा मतदान देने वालॉ के 2/3 संख्या को विशेष बहुमत कहा गया है
[ख]
अनु 368 के अनुसार– संशोधन बिल सदन के उपस्थित तथा सदन मे मत देने वालो के 2/3 संख्या जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो [लोकसभा मे 273 सदस्य]इस बहुमत से संविधान संशोधन ,न्यायधीशॉ को पद से हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना ,राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना अथवा विच्छेदन की मांंग के प्रस्ताव पारित किये जाते है
[ग]
अनु 61 के अनुसार– केवल राष्ट्रपति के महाभियोग हेतु सदन के कुल संख्या का कम से कम 2/3 [लोकसभा मे 364 सदस्य होने पर]
लोकसभा के सत्र
– अनु 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दो सत्रॉ के मध्य 6 मास
से अधिक अंतर ना हो पंरपरानुसार संसद के तीन नियमित सत्रॉ तथा विशेष सत्रों मे आयोजित की जाती है
सत्रॉ का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है
1. बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है सामान्यत फरवरी मई के मध्य चलता है यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है इसी सत्र मे बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है सत्र के प्रांरभ मे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है
2. मानसून सत्र जुलाई अगस्त के मध्य होता है
3. शरद सत्र नवम्बर दिसम्बर के मध्य होता है सबसे कम समयावधि का सत्र होता है
विशेष सत्र – इस के दो भेद है 1. संसद के विशेष सत्र.
2. लोकसभा के विशेष सत्र
संसद के विशेष सत्र – मंत्रि परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इनका आयोजन करता है ये किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक आयोजित किये जाते है
एक विशेष सत्र मे कोई विशेष कार्य चर्चित तथा पारित किया जाता है यदि सदन चाहे भी तो अन्य कार्य नही कर सकता है
लोकसभा का विशेष सत्र– अनु 352 मे इसका वर्णन है किंतु इसे 44 वें संशोधन 1978 से स्थापित किया गया है यदि
लोकसभा के कम से कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव लाते है जिसमे राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने
की बात कही गयी है तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जायेगा
सत्रावसान– मंत्रिपरिषद की सलाह पे सदनॉ का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है इसमे संसद का एक सत्र समाप्त
हो जाता है तथा संसद दुबारा तभी सत्र कर सकती है जब राष्ट्रपति सत्रांरभ का सम्मन जारी कर दे सत्रावसान की दशा मे संसद के
समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नही हो जाते है
स्थगन– किसी सदन के सभापति द्वारा सत्र के मध्य एक लघुवधि का अन्तराल लाया जाता है इस से
सत्र समाप्त नही हो जाता ना उसके समक्ष लम्बित कार्य समाप्त हो जाते है यह दो प्रकार का होता है
1. अनिश्चित कालीन 2. जब अगली मीटिग का समय दे दिया जाता है
लोकसभा का विघटन— राष्ट्रपति द्वारा मंत्रि परिष्द की सलाह पर किया है इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है इसके बाद आमचुनाव ही होते है विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते है समाप्त हो जाते है किंतु बिल जो राज्यसभा मे लाये गये हो और वही लंबित होते है समाप्त न्ही होते या या बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वे भी समापत नही होते है या राष्ट्रपति संसद के दोनॉ सदनॉ की लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले
विधायिका संबंधी कार्यवाही
/प्रक्रियाबिल/विधेयक के प्रकार कुल 4 प्रकार होते है
1.
सामान्य बिल
– इसकी 6 विशेषताएँ है
1. परिभाषित हो
2. राष्ट्रपति की अनुमति हो
3. बिल कहाँ प्रस्तावित हो
4. सदन की विशेष शक्तियॉ मे आता हो
5.कितना बहुमत चाहिए
6. गतिवरोध पैदा होना
यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए
इस बिल को पारित करने मे दोनो सदनॉ की विधायी शक्तिय़ाँ बराबर होती है इसे पारित करने मे सामान्य बहुमत
चाहिए एक सदन द्वारा अस्वीकृत कर देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये तो राष्ट्रपति दोनो सद्नॉ की संयुक्त बैठक मंत्रि परिषद की
सलाह पर बुला लेता है
राष्ट्रपति के समक्ष यह विधेयक आने पर वह इस को संसद को वापस भेज सकता है या स्वीकृति दे सकता है या अनिस्चित काल हेतु रोक सकता है
धन बिल
विधेयक जो पूर्णतः एक या अधिक मामलॉ जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 मे किया गया हो से जुडा हो धन बिल कहलाता है ये मामलें है
1. किसी कर को लगाना,हटाना, नियमन
2. धन उधार लेना या कोई वित्तेय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले
3. भारत की आपात/संचित निधि से धन की निकासी/जमा करना
4.संचित निधि की धन मात्रा का निर्धारण
5. ऐसे व्यय जिन्हें भारत की संचित निधि पे भारित घोषित करना हो
6. संचित निधि मे धन निकालने की स्वीकृति लेना
7. ऐसा कोई मामला लेना जो इस सबसे भिन्न हो
धन बिल केवल लोकसभा मे प्रस्तावित किए जा सकते है इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवशय्क है इन्हें पास करने के लिये सदन का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है
धन बिल मे ना तो राज्य सभा संशोधन कर सकती है न अस्वीकार
जब कोई धन बिल लोकसभा पारित करती है तो स्पीकर के प्रमाणन के साथ यह बिल राज्यसभा मे ले जाया जाता है राज्यसभा इस
बिल को पारित कर सकती है या 14 दिन के लिये रोक सकती है किंतु उस के बाद यह बिल दोनॉ
सदनॉ द्वारा पारित माना जायेगा राज्य सभा द्वारा सुझाया कोई भी संशोधन लोक सभा की इच्छा पे निर्भर करेगा कि वो स्वीकार करे
या ना करे जब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा तो वह सदैव इसे स्वीकृति दे देगा
फायनेसियल बिलवह विधेयक जो एक या अधिक मनीबिल प्रावधानॉ से पृथक हो तथा गैर मनी मामलॉ से भी संबधित हो एक फाइनेंस विधेयक मे धन प्रावधानॉ के साथ साथ सामान्य विधायन से जुडे मामले भी होते है इस प्रकार के विधेयक को पारित करने की शक्ति दोनो सदनॉ मे समान होती
संविधान संशोधन विधेयक
अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
विधेयक पारित करने मे आया गतिरोध
जब संसद के दोनॉ सदनॉ के मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा अस्वीकृत कर दे या इस तरह के संशोधन कर दे जिसे मूल सदन अस्वीकर कर दे या इसे 6 मास तक रोके रखे तब सदनॉ के मध्य गतिवरोध की स्थिति जन्म लेती है अनु 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस दशा मे दोनॉ सदनॉ की संयुक्त बैठक बुला लेगा जिसमे सामान्य बहुमत से फैसला हो जायेगा अब तक मात्र तीन अवसरॉ पे इस प्रकार की बैठक बुलायी गयी है
1. दहेज निषेध एक्ट 1961
2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978
3.पोटा एक्ट 2002
संशोधन के विरूद्ध सुरक्षा उपाय 1. न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र है
2.संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध न हो
3. संसद की संशोधन शक्ति के भीतर आता हो
4. संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन तीनॉ अंगो का संतुलन बना रहे
5. संघ के ढाँचे से जुडा होने पर आधे राज्यॉ की विधायिका से स्वीकृति मिले
6. गठबंधन राजनीति भी संविधान संशोधन के विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय देती है क्योंकि एकदलीय पूर्ण बहुमत के दिन समाप्त हो चुके
अध्यादेश जारी करना
अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पे नियंत्रण
1. प्रत्येक जारी किया हुआ अध्यादेश संसद के दोनो सदनो द्वारा उनके सत्र शुरु होने के 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृत करवाना होगा इस प्रकार कोई अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बिना 6 मास + 6 सप्ताह से अधिक नही चल सकता है
2. लोकसभा एक अध्यादेश को अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पूर्व पास कर सकती है
3. राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यायिक समीक्षा का विषय़ हो सकता है
संसद मे राष्ट्रपति का अभिभाषण
यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
अभिभाषण मे सरकार की उपलब्धियॉ तथा नीतियॉ का वर्णन तथा समीक्षा होती है[जो पिछले वर्ष मे हुई थी] आतंरिक समस्याओं से जुडी नीतियाँ भी इसी मे घोषित होती है प्रस्तावित विधायिका कार्यवाहिया जो कि संसद के सामने उस वर्ष के सत्रॉ मे लानी हो का वर्णन भी अभिभाषण मे होता है अभिभाषण के बाद दोनो सद्न पृथक बैठक करके उस पर चर्चा करते है जिसे पर्यापत समय दिया जाता है
संचित निधि
– संविधान के अनु 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस मे समस्त एकत्र कर/राजस्व जमा,लिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता हैsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai.
भारत की लोक निधि
--- अनु 266 इसका वर्णन भी करता है वह धन जिसे भारत सरकार कर एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋण के अलावा एकत्र करे भारत की लोकनिधि कहलाती है कर्मचारी भविष्य़ निधि को भारत की लोकनिधि मे जमा किया गया है यह कार्यपालिका के अधीन निधि है इससे व्यय धन महालेखानियंत्रक द्वारा जाँचा जाता है अनु 266 राज्यॉ की लोकनिधि का भी वर्णन करता है
भारत की आपातकाल निधि
--- अनु 267 संसद को निधि जो कि आपातकाल मे प्रयोग की जा सकती हो स्थापित करने का अधिकार देता है यह निधि राष्ट्रपति के अधीन है इससे खर्च धन राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है परंतु संसद के समक्ष इसकी स्वीकृति ली जाती है यदि संसद स्वीकृति दे देती है तो व्यय धन के बराबर धन भारत की संचित निधि से निकाल कर इसमे डाल दिया जाता है अनु 267 राज्यॉ को अपनी अपनी आपातकाल निधि स्थापित करने का अधिकार भी देता है
भारित व्यय
--- वे व्यय जो कि भारत की संचित निधि पर बिना संसदीय स्वीकृति के भारित होते है ये व्यय या तो संविधान द्वारा स्वीकृत होते है या संसद विधि बना कर डाल देती है कुछ संवैधानिक पदॉ की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये यह व्यय प्रयोग लाये गये है अनु 112[3] मे कुछ भारित व्ययॉ की सूची है
1. राष्ट्रपति के वेतन,भत्ते,कार्यालय से जुडा व्यय है
2. राज्यसभा लोकसभा के सभापतियॉ उपसभापतियॉ के वेतन भत्ते
3.ऋण भार जिनके लिये भारत सरकार उत्तरदायी है [ब्याज सहित]
4.सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन भत्ते पेंशन तथा उच्च न्यायालय की पेंशने इस पर भारित है
5. महालेखानियंत्रक तथा परीक्षक [केग] के वेतन भत्ते
6. किसी न्यायिक अवार्ड/डिक्री/निर्णय के लिये आवशयक धन जो न्यायालय/ट्रिब्न्यूल द्वारा पारित हो
7. संसद द्वारा विधि बना कर किसी भी व्यय को भारित व्यय कहा जा सकता है
अभी तक संसद ने निर्वाचन आयुक्तॉ के वेतन भत्ते पेंशन ,
केन्द्रीय सर्तकता आयोगसदस्यॉ के वेतन भत्ते पेंशन भी इस पर भारित किये है
वित्त व्यवस्था पर संसद का नियंत्रण
अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है
अनु 112 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा को संसद के सामने रखेगा यह वित्तीय लेखा ही बजट है<br /
बजट
1. अनुमानित आय व्यय जो कि भारत सरकार ने भावी वर्ष मे करना हो
2. यह भावी वर्ष के व्यय के लिये राजस्व उगाहने का वर्णन करता है
3. बजट मे पिछले वर्ष के वास्तविक आय व्यय का विवरण होता है
बजट सामान्यत वित्तमंत्री द्वारा सामान्यतः फरवरी के आखरी दिन लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता है उसी समय राज्यसभा मे भी बजट के कागजात रखे जाते है यह एक धन बिल है
कटौती प्रस्ताव
—बजट प्रक्रिया का ही भाग है केवल लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता है ये वे उपकरण है जो लोकसभा सदस्य कार्यपालिका पे नियंत्रण हेतु उपयोग लाते है ये अनुदानॉ मे कटौती कर सकते है इसके तीन प्रकार है
1.
नीति सबंधी कटौती--- इस प्रस्ताव का ल्क्ष्य लेखानुदान संबंधित नीति की अस्वीकृति है यह इस रूप मे होती है ‘-------‘ मांग को कम कर मात्र 1 रुपया किया जाता है यदि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाये तो यह सरकार की नीति संबंधी पराजय मानी जाती है उसे तुरंत अपना विश्वास सिद्ध करना होता है
2.
किफायती कटौती--- भारत सरकार के व्यय को उससीमा तक कम कर देती है जो संसद के मतानुसार किफायती होगी यह कटौती सरकार की नीतिगत पराजय नहीं मानी जाती है
3.
सांकेतिक कटौती--- इन कटौतीयों का ल्क्ष्य संसद सदस्यॉ की विशेष शिकायतें जो भारत सरकार से संबंधित है को निपटाने हेतु प्रयोग होती है जिसके अंतर्गत मांगे गये धन से मात्र 100 रु की कटौती की जाती है यह कटौती भी नीतिगत पराजय नही मानी जाती है
लेखानुदान (वोट ओन अकाउंट)
अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
वोट ओन क्रेडिट [प्रत्यानुदान] लोकसभा किसी ऐसे व्यय के लिये धन दे सकती है जिसका वर्णन किसी पैमाने या किसी सेवा मद मे रखा जा सक्ना संभव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे उस पर व्यय होता है उसे किस शीर्षक के अंतर्गत रखे?यह लोकसभा द्वारा पारित खाली चैक माना जा सकता है आज तक इसे प्रयोग नही किया जा सका है
जिलेटीन प्रयोग—समयाभाव के चलते लोकसभा सभी मंत्रालयों के व्ययानुदानॉ को एक मुश्त पास कर देती है उस पर कोई चर्चा नही करती है यही जिलेटीन प्रयोग है यह संसद के वित्तीय नियंत्रण की दुर्बलता दिखाता है
संसद मे लाये जाने वाले प्रस्ताव
अविश्वास प्रस्ताव
लोकसभा के क्रियांवयन नियमॉ मे इस प्रस्ताव का वर्णन है विपक्ष यह प्रस्ताव लोकसभा मे मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाता है इसे लाने हेतु लोकसभा के 50 सद्स्यॉ का समर्थन जरूरी है यह सरकार के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपॉ का वर्णन नही करता है केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद मे विश्वास नही करता है एक बार प्रस्तुत करने पर यह प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्ताव के सभी अन्य प्रस्तावॉ पर प्रभावी हो जाता है इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है इस पर् चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यॉ नीतियॉ की चर्चा हो सकती है लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है संसद के एक सत्र मे एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सकते है
विश्वास प्रस्ताव--- लोकसभा नियमॉ मे इस प्रस्ताव का कोई वर्णन नही है यह आवश्यक्तानुसार उत्पन्न हुआ है ताकि मंत्रिपरिषद अपनी सत्ता सिद्ध कर सके यह सदैव मंत्रिपरिषद लाती है इसके गिरजाने पर उसे त्याग पत्र देना पडता है
निंदा प्रस्ताव--- लोकसभा मे विपक्ष यह प्रस्ताव लाकर सरकार की किसी विशेष नीति का विरोध/निंदा करता है इसे लाने हेतु कोई पूर्वानुमति जरूरी नही है यदि लोकसभा मे पारित हो जाये तो मंत्रिपरिषद निर्धारित समय मे विश्वास प्रस्ताव लाकर अपने स्थायित्व का परिचय देती है है उसके लिये यह अनिवार्य है
कामरोको प्रस्ताव--- लोकसभा मे विपक्ष यह प्रस्ताव लाता है यह एक अद्वितीय प्रस्ताव है जिसमे सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर तात्कालीन जन मह्त्व के किसी एक मुद्दे को उठाया जाता है प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पे निंदा प्रस्ताव के समान प्रभाव छोडता है
संघीय न्यायपालिका
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति
29 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान का वर्णन संविधान मे है अनु 124[2] के अनुसार् मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इच्छानुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार
सर्वोच्च न्यायालयउच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा वही अन्य जजॉ की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी
सर्वोच्च न्यायालयएडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजों के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नहीं होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनः विचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा यद्यपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्ठम न्यायधीशों की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित में होगी
बाद में अपना मत बदलते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 जजों के साथ सलाह करना अनिवार्य कर दिया था वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेषित नहीं करेगा यदि दो या ज्यादा जजों की सलाह इस्के विरूद्ध हो किंतु 4 जजों की सलाह उसे अन्य जजों जिनसे वो चाहे सलाह लेने से नहीं रोकेगी
न्यायपालिका के न्यायधीशों की पदच्युति
—इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
1. संसद के किसी भी सदन मे प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकस्भा मे 100 राज्यसभा मे 50 सद्स्यॉ का समर्थन अनिवार्य है
2. प्रस्ताव मिलने पे सदन का सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जाँच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इस की जाँच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी यदि इस मे जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नही कर सकता है
अभी तक सिर्फ एक बार किसी जज के विरूद्ध जांच की गयी है जज रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गये थे किंतु संसद मे आवश्यक बहुमत के अभाव के चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका था
अभिलेख न्यायालय
अनुच्छेद 129
उच्चतम न्यायालयको तथा अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है यह संकल्पना अंग्रेजी विधि से ली गयी है अभिलेख न्यायालय का अर्थ अनु 129 सुप्रीम कोर्ट को तथा अनु 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है यह संकल्पना इंग्लिश विधि से ली गयी है
अभिलेख न्यायालय का अर्थ1. न्यायालय की कार्यवाही तथा निर्णय को दूसरे न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किया जा सकेगा
2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक जब कोई व्यक्ति आदेश निर्देश का पालन न करे या उल्लंघ न करे तो यह सिविल अवमानना है पर्ंतु यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को बदनाम करे जजों को बदनाम तथा विवादित बताने का प्रयास करे तो यह आपराधिक अवमानना होगी जिसके लिये कारावास/जुर्माना दोनो देना पडेगा वही सिविल अवमानना मे कारावास सम्भव नहीं है यह शक्ति भारत मे काफी कुख्यात तथा विवादस्पद है
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ
अनु 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मे होगा पर्ंतु यह भारत मे और कही भी मुख्य न्यायाधीश् के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा
क्षेत्रीय खंडपीठों का प्रश्न- विधि आयोग अपनी रिपोर्ट के माध्यम से क्षेत्रीय खंडपीठों के गठन की अनुसंशा कर चुका है न्यायालय के वकीलॉ ने भी प्राथर्ना की है कि वह अपनी क्षेत्रीय खंडपीठों का गठन करे ताकि देश के विभिन्न भागॉ मे निवास करने वाले वादियॉ के धन तथा समय दोनॉ की बचत हो सके,किंतु न्यायालय ने इस प्रश्न पे विचार करने के बाद निर्णय दिया है कि पीठॉ के गठन से
1. ये पीठे क्षेत्र के राज नैतिक दबाव मे आ जायेगी
2. इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एकात्मक चरित्र तथा संगठन को हानि पहुँच सकती है
किंतु इसके विरोध मे भी तर्क दिये गये है
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
जनहित याचिकाएँ
– इस प्रकार की याचिकाओँ का विचार अमेरिका ए जन्मा वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कह्ते है यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायधीश निर्मित विधि है
जनहित याचिका भारत मे
पी.एन.भगवतीने प्रारंभ की थी ये याचिकाँए जनहित को सुरक्षित तथा बढाना चाहती है ये लोकहित भावना पे कार्य करती है
ये ऐसे न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है इनका ल्क्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है
ये समूह हित मे काम आती है ना कि व्यक्ति हित मे यदि इनका दुरूपयोग किया जाये तो याचिकाकर्ता पे जुर्माना तक किया जा सकता है इनको स्वीकारना या ना स्वीकारना न्यायालय पे निर्भर करता है
इनकी स्वीकृति हेतु सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाये है
1. लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति,संगठन इन्हे ला सकता है
2. कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट याचिका मान कर ये जारी की जा सकती है
3. कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे
4. ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरूद्ध भी लायी जा सकती है
इसके लाभ1. इस याचिका से जनता मे स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे मे चेतना बढती है यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को वृहद बनाती है इसमे व्यक्ति को कई नये अधिकार मिल जाते है
2. यह कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिये बाधित करती है ,साथ ही यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिशिचतता करती है
आलोचनाएं 1. ये सामान्य न्यायिक संचालन मे बाधा डालती है
2. इनके दुरूपयोग की प्रवृति परवान पे है
इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ बन्धन इनके प्रयोग पे लगाये है
न्यायिक सक्रियता
न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा निभायी जाने वाली वह सक्रिय भूमिका है जिसमे राज्य के अन्य अंगों को उनके संवैधानिक कृत्य करने को बाधय करे यदि वे अंग अपने कृत्य संपादित करने मे सफल रहे तो जनतंत्र तथा विधि शासन के लिये न्यायपालिका उनकी शक्तियों भूमिका का निर्वाह सीमित समय के लिये करेगी यह सक्रियता जनतंत्र की शक्ति तथा जन विश्वास को पुर्नस्थापित करती है
इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है
इसका समर्थन एक सीमित सीमा तक ही किया जा सकता है इसके विरोध के स्वर भी आप कार्य पालिका तथा विधायिका मे सुन सकते है इसके चलते ही हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने खुद संयम बरतने की बात सवीकारी है तथा कई मामलों मे हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है
संविधान विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका
एक तरफ यह संविधान का संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्ता, मौलिक अधिकारों का रक्षक ,केन्द्र-राज्य विवादों मे एक मात्र मध्यस्थ है वहीँ यह संविधान के विकास मे भी भूमिका निभाता रहा है इसने माना है कि निरंतर संवैधानिक विकास होना चाहिए ताकि समाज के हित संवर्धित हो ,न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के कारण यह संवैधानिक विकास मे सहायता करता है सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारत मे संविधान सर्वोच्च है इसने संविधान के मूल ढाँचे का अदभुत सिद्धांत दिया है जिसके चलते संविधान काफी सुरक्षित हो गया है इसे मनमाने ढंग से बदला नही जा सकता ह
ै इसने मौलिक अधिकारों का विस्तार भी किया है इसने अनु 356 के दुरूपयोग को भी रोका है
उच्चतम न्यायालयइस उक्ति का पालन करता है कि संविधान खुद नहीं बोलता है यह अपनी वाणी न्यायपालिका के माध्यम से बोलता है
संविधान भाग 6
पाठ 1 राज्य कार्यपालिका
राज्यपालराज्यपाल् कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह राज्य मे केन्द्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पे बना रहता है वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है
उसका पद तथा भूमिका भारतीय राजनीति मे दीर्घ काल से विवाद का कारण रही है जिसके चलते काफी विवाद हुए है
सरकारिया आयोगने अपनी रिपोर्ट मे इस तरह की सिफारिश दी थी
1. एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति करे
2. वह जीवन के किसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो
3. वह राज्य के बाहर का रहने वाला हो
4. वह राजनैतिक रूप से कम से कम पिछले 5 वर्शो से राष्ट्रीय रूप से सक्रिय ना रहा हो तथा नियुक्ति वाले राज्य मे कभी भी सक्रिय ना रहा हो
5. उसे सामान्यत अपने पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दिया जाये ताकि वह निष्पक्ष रूप से काम कर सके
6. केन्द्र पर सत्तारूढ राजनैतिक गठबन्धन का सद्स्य ऐसे राज्य का राज्यपाल नही बनाया जाये जो विपक्ष द्वारा शासित हो
7. राज्यपाल द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रथा जारी रहनी चाहिए
8. यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को अनु 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करे तो उसे उन कारणॉ ,स्थितियों का वर्णन रिकार्ड मे रखना चाहिए जिनके आधार पे वह इस निष्क़र्ष पे पहुँचा हो
इसके अलावा राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है जो अपने कर्तव्य मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से करता है परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति उसकी मंत्रिपरिषद की तुलना मे बहुत सुरक्षित है वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं है राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही है जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है किंतु संविधान राजयपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है उसका पद उतना ही शोभात्मक है उतना ही कार्यातमक भी है
राज्यपाल उन सभी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग भी करता है जो राष्ट्रपति को मिलती है इसके अलावा वो इन अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग भी करता है
अनु 166[2] के अंर्तगत यदि कोई प्रशन उठता है कि राजयपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है
अनु 166[3] राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिनसे राज्यकार्यों को सुगमता पूर्वक संचालन हो साथ ही वह मंत्रियों मे कार्य विभाजन भी कर सकता है
अनु 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने मे कर सकता है
अनु 356 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता हो
विशेष विवेकाधीन शक्तिपंरपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट के सम्बन्ध मे निर्णय ले सकता है कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो ले किंतु इसे मानने हेतु वह बाध्य ना हो और ना ही उसे सलाह लेने की जरूरत पडती हो
राज्य विधायिका
संविधान मे 6 राज्यों हेतु द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है
उपरी सदन स्थापना तथा उन्मूलन अनु 169 के अनुसार यह शक्ति केवल संसद को है
ऊपरी सदन का महत्व–यह सदन प्रथम श्रेणी का नही होता यह विधान सभा द्वारा पारित बिल को अस्वीकृत संशोधित नहीं कर सकता है केवल किसी बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 मास के लिये रोक सकता है इसके अलावा मंत्रिपरिषद मे विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु इसका प्रयोग हो सकता है क्योंकि यहाँ मनोनीत सदस्यों की सुविधा भी है
विधायिका की प्रक्रियाएँ तीन प्रकार के बिल धन ,फाइनेंस तथा सामान्य होते है ,धन बिल संसद की तरह ही पास होते है ,फाइनेंस बिल केवल निचले सदन मे ही पेश होते है , सामान्य बिल जो ऊपरी सदन मे पेश होंगे व पारित हो यदि बाद मे निचले सदन मे अस्वीकृत हो जाये तो समाप्त हो जाते है
निचले सदन द्वारा पारित बिल को ऊपरी सदन केवल 3 मास के लिये रोक सकता है उसके बाद वे पारित माने जाते है
राज्य न्यायपालिका
राज्य न्यायपालिका मे तीन प्रकार की पीठें होती है एकल जिसके निर्णय को उच्च न्यायालय की डिवीजनल/खंडपीठ/
सर्वोच्च न्यायालयमे चुनौती दी जा सकती है
खंड पीठ 2 या 3 जजों के मेल से बनी होती है जिसके निर्णय केवल
उच्चतम न्यायालयमें चुनौती पा सकते हैं
संवैधानिक/फुल बेंच सभी संवैधानिक व्याख्या से संबधित वाद इस प्रकार की पीठ सुनती है इसमे कम से कम पाँच जज होते हैं
अधीनस्थ न्यायालय
इस स्तर पर सिविल आपराधिक मामलों की सुनवाई अलग अलग होती है इस स्तर पर सिविल तथा सेशन कोर्ट अलग अलग होते है इस स्तर के जज सामान्य भर्ती परीक्षा के आधार पर भर्ती होते है उनकी नियुक्ति राज्यपाल राज्य मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है
फास्ट ट्रेक कोर्ट– ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है
ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है
इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
आलोचना 1. निर्धारित संख्या मे गठन नहीं हुआ
2. वादों का निर्णय संक्षिप्त ढँग से होता है जिसमें अभियुक्त को रक्षा करने का पूरा मौका नहीं मिलता है
3. न्यायधीशों हेतु कोई सेवा नियम नहीं है
लोक अदालत -- जनता की अदालतें है ये नियमित कोर्ट से अलग होती है पदेन या सेवानिवृत जज तथा दो सदस्य एक सामाजिक कार्यकता ,एक वकील इसके सद्स्य होते है सुनवाई केवल तभी करती है जब दोनों पक्ष इसकी स्वीकृति देते हो ये बीमा दावों क्षतिपूर्ति के रूप वाले वादों को निपता देती है
इनके पास वैधानिक दर्जा होता है वकील पक्ष नहीं प्रस्तुत करते हैं
इनके लाभ– 1.न्यायालय शुल्क नहीं लगते
2. यहाँ प्रक्रिया संहिता/साक्ष्य एक्ट नहीं लागू होते
3. दोनों पक्ष न्यायधीश से सीधे बात कर समझौते पर पहुचँ जाते है
4. इनके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं ला सकते है
आलोचनाएँ 1. ये नियमित अंतराल से काम नहीं करती है
2. जब कभी काम पे आती है तो बिना सुनवाई के बडी मात्रा मे मामले निपटा देती है
3. जनता लोक अदालतों की उपस्थिति तथा लाभों के प्रति जागरूक नहीं है
जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति
संवैधानिक प्रावधान स्वतः जम्मू तथा कश्मीर पे लागू नहीं होते केवल वहीं प्रावधान जिनमे स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वे जम्मू कश्मीर पे लागू होते है उस पर लागू होते है
जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का ज्ञान इन तथ्यों से होता है
1. जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधान से वहाँ का कार्य चलता है ये संविधान जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य की नागरिकता भी देता है केवल इस राज्य के नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते है या चुनाव लड सकते है या सरकारी सेवा ले सकते है
2. संसद जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाला ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो इसकी राज्य सूची का विषय हो
3. अवशेष शक्ति जम्मू कश्मीर विधान सभा के पास होती है
4. इस राज्य पर सशस्त्र विद्रोह की दशा मे या वित्तीय संकट की दशा मे आपात काल लागू नहीं होता है
5. संसद राज्य का नाम क्षेत्र सीमा बिना राज्य विधायिका की स्वीकृति के नहीं बदलेगीं
6. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य मुख्यमंत्री की सलाह के बाद करेगी
7. संसद द्वारा पारित निवारक निरोध नियम राज्य पर अपने आप लागू नहीं होगा
8. राज्य की पृथक दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता है
९।
केन्द्र राज्य संबंध
विधायिका स्तर पर सम्बन्ध
संविधान की सातंवी अनुसूची विधायिका के विषय़ केन्द्र राज्य के मध्य विभाजित करती है संघ सूची मे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय़ है
राज्यों पर केन्द्र का विधान संबंधी नियंत्रण1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
2. अनु 31[ब] के द्वारा नौवीं अनुसूची भी जोडी गयी है तथा उन सभी अधिनियमों को जो राज्य विधायिका द्वारा पारित हो तथा अनुसूची के अधीन रखें गये हो को भी न्यायिक पुनरीक्षा से छूट मिल जाती है लेकिन यह कार्य संसद की स्वीकृति से होता है
3. अनु 200 राज्य का राज्यपाल धन बिल सहित बिल जिसे राज्य विधायिका ने पास किया हो को राष्ट्रपति की सहमति के लिये आरक्षित कर सकता है
4. अनु 288[2] राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणों पर नहीं देता जो कि जल संग्रह, विधुत उत्पादन, तथा विधुत उपभोग ,वितरण ,उपभोग, से संबंधित हो ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति पायेगा
5. अनु 305[ब] के अनुसार राज्य विधायिकाको शक्ति देता है कि वो अंतराज्य व्यापार वाणिज़्य पर युक्ति निर्बधंन लगाये परंतु राज्य विधायिका मे लाया गया बिल केवल राष्ट्रप्ति की अनुशंसा से ही लाया जा सकता है
केन्द्र राज्य प्रशासनिक संबंध
अनु 256के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ इस तरह प्रयोग लायी जाये कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके । इस तरह संसद की विधि के अधीन विधिंयों का पालन हो सके । इस तरह संसद की विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गयी है । केन्द्र राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इस संबंध मे आवश्यक हो
अनु 257 ----- कुछ मामलों मे राज्य पर केन्द्र नियंत्रण की बात करता है । राज्य कार्यपालिका शक्ति इस तरह प्रयोग ली जाये कि वह संघ कार्यपालिका से संघर्ष ना करे केन्द्र अनेक क्षेत्रों मे राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति कैसे प्रयोग करे इस पर निर्देश दे सकता है यदि राज्य निर्देश पालन मे असफल रहा तो राज्य मे राष्ट्रपति शासन तक लाया जा सकता है
अनु 258[2] के अनुसार --- संसद को राज्य प्रशासनिक तंत्र को उस तरह प्रयोग लेने की शक्ति देता है जिनसे संघीय विधि पालित हो केन्द्र को अधिकार है कि वह राज्य मे बिना उसकी मर्जी के सेना, केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात कर सकता है
अखिल भारतीय सेवाएँ भी केन्द्र को राज्य प्रशासन पे नियंत्रण प्राप्त करने मे सहायता देती है अनु 262 संसद को अधिकार देता है कि वह अंतराज्य जल विवाद को सुलझाने हेतु विधि का निर्माण करे संसद ने अंतराज्य जल विवाद तथा बोर्ड एक्ट पारित किये थे
अनु 263 राष्ट्राप्ति को शक्ति देता है कि वह अंतराज्य परिषद स्थापित करे ताकि राज्यों के मध्य उत्पन्न मत विभिन्ंता सुलझा सके
निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली/कार्य
1 निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनॉ का पर्यवेक्षण ,निर्देशन तथा आयोजन करवाये वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ,संसद,राज्यविधानसभा के चुनाव करता है
2 निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है
3 राजनैतिक दलॉ का पंजीकरण करता है
4. राजनैतिक दलॉ का राष्ट्रीय ,राज्य स्तर के दलॉ के रूप मे वर्गीकरण ,मान्यता देना, दलॉ-निर्दलीयॉ को चुनाव चिन्ह देना
5. सांसद/विधायक की अयोग्यता[दल बदल को छोडकर]पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देना
6. गलत निर्वाचन उपायॉ का उपयोग करने वाले व्यक्तियॉ को निर्वाचन के लिये अयोग्य घोषित करना
निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ अनु 324[1] निर्वाचन आयोग को निम्न शक्तियाँ देता है
1. सभी निर्वाचनॉ का पर्यवेक्षण ,नियंत्रण,आयोजन करवाना
2.सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण ,निर्देशन ,नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए
निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है
निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक है न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरूद्ध प्रयोग नही की जा सकती है
यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है
सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है
जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 14,15 भी राष्ट्रपति,राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते है
भारत मे निर्वाचन सुधार
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन किये गये हैं.
1. इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा. वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव मे इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ
2. राजनैतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा यदि वह चुनाव लडना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन करे तथा उनका समावेश अपने दलीय संविधान मे करे
3. मतदान केन्द्र पर कब्जा, जाली मत
त्रुटियां
परस्पर वीरोधी, मिलकत या संपदा का अधिकार मूल अधिकार रहा । कई साल तक शिक्षा का मूल अधिकार न होकर नीति के निदेशक के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि होती रही ओर गरीब, गरीब होते रहें ।
फेडरेशन तथा कनफेडरेशन का भेद
फेडरेशन
- दो या अधिक संघटको का औपचारिक संगठन
- सम्प्रभु तथा स्वतंत्र परंतु उसके संघटक सम्प्रभु तथा स्वतंत्र नही होते
- संघटक संघ से स्वतंत्र होने की शक्ति नही रखते है
- संघ तथा उसके निवासियो के मध्य वैधानिक सम्बन्ध होता है [नागरिकता] नागरिको के अधिकार तथा कर्तव्य होते है
कनफेडरेशन
- दो या अधिक संघटको का ढीला संघठन [रास्त्र मन्डल ]
- संघटक सम्प्रभु तथा स्वतंत्र होते है परंतु खुद कनफेडरेशन मे ये गुण नही होते है
- संघटक स्वतंत्र होने की शक्ति रखते है
- निवासी परिसंघ के नागरिक नही होते बल्कि उसके संघट्को के नागरिक होते है
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
यह सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक
मान्टेस्कयूने दिया था उसके अनुसार राज्य की शक्ति उसके तीन भागो कार्य , विधान, तथा न्यायपालिकाओ मे बांट देनी चाहिये
ये सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है
अमेरिकी सविन्धान पहला ऐसा सविन्धान था जिस मे ये सिद्धांत अपनाया गया था
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय सविन्धान मे------सविन्धान मे इसका साफ वर्णन ना होकर सकेत मात्र है इस हेतु सविन्धान मे तीनो अंगो का पृथक वर्णन है संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत मे कार्यपालिका तथा विधायिका मे पूरा अलगाव नही हो सका है कार्यपालिका[मंत्रीपरिषद] विधायिका मे से ही चुनी जाती है तथा उसके निचले सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है
अनु 51 के अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए इस लिये ही 1973 मे दंड प्रक्रिया सन्हिता पारित की गयी जिस के द्वारा जिला मजिस्टृटो की न्यायिक शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्टृटो को दे दी गयी थी
बाहरी कडियाँ
[दिखाएँ]भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम भारत
भारत