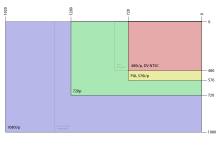प्रस्तुति-- धीरज पांडेय, गणेश प्रसाद
फीचर
फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर फीचर कहा जाता है। हिन्दी में फीचर के लिये रुपक शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन फीचर के लिये हिन्दी में प्रायः फीचर शब्द का ही प्रयोग होता है। फीचर का सामान्य अर्थ होता है – किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है। लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नही होता है।
फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव – जन्तु, तीज – त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति – परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है।
फीचर के प्रकार
· व्यक्तिपरक फीचर
· सूचनात्मक फीचर
· विवरणात्मक फीचर
· विश्लेषणात्मक फीचर
· साक्षात्कार फीचर
· इनडेप्थ फीचर
· विज्ञापन फीचर
· अन्य फीचर
फीचर की विशेषतायें
· किसी घटना की सत्यता या तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना चाहिये।
· फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिये।
· फीचर का विषय रोचक होना चाहिये या फीचर को किसी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिये।
· फीचर को शुरु से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिये।
· फीचर को ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तनसूचक होना चाहिये।
· फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिये।
· फीचर लेखक किसी घटना की सत्यता या तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील करता है।
· फीचर को सीधा सपाट न होकर चित्रात्मक होना चाहिये।
· फीचर कीभाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ – साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिये।
फीचर लेखन की प्रक्रिया
· विषय का चयन
· सामग्री का संकलन
· फीचर योजना
विषय का चयन
किसी भी फीचर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला है। इसलिये फीचर का विषय समयानुकूल, प्रासंगिक और समसामयिक होना चाहिये। अर्थात फीचर का विषय ऐसा होना चाहिये जो लोक रुचि का हो, लोक – मानव को छुए, पाठकों में जिज्ञासा जगाये और कोई नई जानकारी दे।
सामग्री का संकलन
फीचर का विषय तय करने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चरण है विषय संबंधी सामग्री का संकलन। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में किसी विषय पर लिखा गया फीचर उबाऊ हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र – पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा फीचर लेखक को बहुत सामग्री लोगों से मिलकर, कई स्थानों में जाकर जुटानी पड़ सकती है।
फीचर योजना
फीचर से संबंधित पर्याप्त जानकारी जुटा लेने के बाद फीचर लेखक को फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध खाका बनाना चाहिये।
फीचर लेखन की संरचना
· विषय प्रतिपादन या भूमिका
· विषय वस्तु की व्याख्या
· निष्कर्ष
विषय प्रतिपादन या भूमिका
फीचर लेखन की संरचना के इस भाग में फीचर के मुख्य भाग में व्याख्यायित करने वाले विषय का संक्षिप्त परिचय या सार दिया जाता है। इस संक्षिप्त परिचय या सार की कई प्रकार से शुरुआत की जा सकती है। किसी प्रसिद्ध कहावत या उक्ति के साथ, विषय के केन्द्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन करके, घटना की नाटकीय प्रस्तुति करके, विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पूछकर। मिका का आरेभ किसी भी प्रकार से किया जाये इसकी शैली रोचक होनी चाहिये मुख्य विष्य का परिचय इस तरह देना चाहिये कि वह पूर्ण भी लगे लेकिन उसमें ऐसा कुछ छूट जाये जिसे जानने के लिये पाठक पूरा फीचर पढ़ने को बाध्य हो जाये।
विषय वस्तु की व्याख्या
फीचर की भूमिका के बाद फीचर के विषय या मूल संवेदना की व्याख्या की जाती है। इस चरण में फीचर के मुख्य विषय के सभी पहलुओं को अलग – अलग व्याख्यायित किया जाना चाहिये। लेकिन सभी पहलुओं की प्रस्तुति में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रमबद्धता होनी चाहिये। फीचर को दिलचस्प बनाने के लिये फीचर में मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि का समावेश करना चाहिये।
निष्कर्ष
फीचर संरचना के इस चरण में व्याख्यायित मुख्य विषय की समीक्षा की जाती है। इस भाग में फीचर लेखक अपने ऴिषय को संक्षिप्त रुप में प्रस्तुत कर पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुये फीचर को समाप्त करता है। साथ ही वह कुछ सवालों को पाठकों के लिये अनुत्तरित भी छोड़ सकता है। और कुछ नये विचार सूत्र पाठकों से सामने रख सकता है जिससे पाठक उन पर विचार करने को बाध्य हो सके।
फीचर संरचना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू
शीर्षक
किसी रचना का यह एक जरुरी हिस्सा होता है और यह उसकी मूल संवेदना या उसके मूल विषय का बोध कराता है। फीचर का शीर्षक मनोरंजक और कलात्मक होना चाहिये जिससे वह पाठकों में रोचकता उत्पन्न कर सके।
छायाचित्र
छायाचित्र होने से फीचर की प्रस्तुति कलात्मक हो जाती है जिसका पाठक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विषय से संबंधित छायाचित्र देने से विषय और भी मुखर हो उठता है। साथ ही छायाचित्र ऐसा होना चाहिये जो फीचर के विषय को मुखरित करे फीचर को कलात्मक और रोचक बनाये तथा पाठक के भीतर विषय की प्रस्तुति के प्रति विश्वसनीयता बनाये।